शिक्षा का मूल आधार
Apr 26, 2019 • 739 views
किसी समाज की शिक्षा तथा उसके उद्देश्य मूल रूप से उसके जीवन दर्शन पर आधारित होते हैं। इसके साथ-साथ वे समाज विशेष की संरचना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसकी राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी आधारित होते हैं। मानव की स्वयं की प्रकृति भी उसकी शिक्षा के स्वरूप को प्रभावित करती है। आज विज्ञान का युग है, शिक्षा युग के प्रभाव से अछूती कैसे रह सकती है! मूल रूप से यह सभी शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम आदि निश्चित करने के आधार हैं।
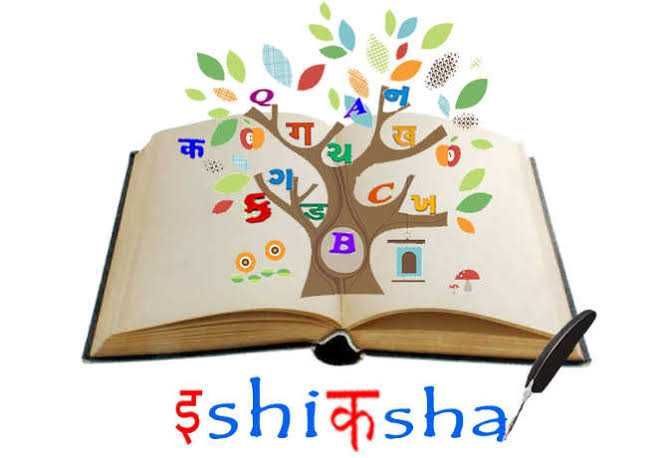
दार्शनिक आधार--------------------------------
इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन का प्रति हमारे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं। कोई इस संसार को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित मानता है, तो कोई इसे प्राकृतिक पदार्थों का परिणाम। आध्यात्मिक विचारधारा के लोग मनुष्य को आत्माधारी मानते हैं। और यह प्रतिपादन करते हैं मनुष्य जीवन का अंतिम उपदेश आत्मा की अनुभूति है। पदार्थवादी दार्शनिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। और वे इस भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान करा देना चाहते हैं जिससे मनुष्य उनका अधिकतम उपयोग करके सुख प्राप्त कर सकें।
समाजशास्त्रीय आधार--------------------------
शिक्षा का मूल आधार समाज तथा उसके जीवन दर्शन को भी माना जा सकता है। समाज विशेष की संरचना, उसकी संस्कृति तथा धार्मिक स्थिति शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने का मुख्य आधार होते हैं। उदाहरण के लिए जिन समाज में स्त्री पुरुषों में भेद किया जाता है और स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रखा जाता है। उन समाजों में स्त्रियों को केवल लिखने-पढ़ने भर की शिक्षा दी जाती है। और जिन समाज में स्त्री पुरुषों में इस प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता उन समाजों में स्त्री पुरुषों की शिक्षा के समान उद्देश्य होते हैं।
राजनैतिक आधार-------------------------------
शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव राज्य और राज्यतंत्र का पड़ता है। जिस समाज में जैसी शासन प्रणाली होती है उसकी शिक्षा तथा उसके उद्देश्य उसी के अनुसार निश्चित होते हैं। जैसे जिस देश में एकतंत्र शासन प्रणाली होती है। उसमें शासक अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करता है और देश को प्रत्येक नागरिक को अपना सच्चा भक्त बनाने का प्रयत्न करता है जिस देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है। उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ का आदर किया जाता है। और उसमें स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास किया जाता है।
आर्थिक आधार---------------------------------
समाज का आर्थिक स्थिति भी उसके शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने के मूल आधार होते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाजों की शिक्षा के उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाज सामान्य शिक्षा की बात ही सोच पाते हैं। निर्धन समाज तो शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कर पाते। परंतु एक बात अवश्य है और वह यह कि कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का समाज अपनी आर्थिक कठिनाइयों से नहीं घबराता और ऐसी शिक्षा का निर्माण करता है जो उसकी आर्थिक समस्याओं के हल करने में सहायक होती है।
मनोवैज्ञानिक आधार----------------------------
एक युग था जब मनुष्य को छोटा प्रौढ़ समझा जाता था। और उसे बचपन से ही उच्च आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी। मनोविज्ञान में मनुष्य की प्रकृति उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया और यह बताया कि पृथ्वी और मानसिक संरचना की दृष्टि से कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते और उसका समस्त विकास उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान और योग्यताओं पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होने लगे हैं।
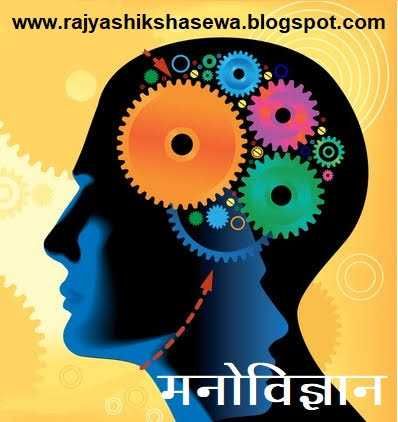
वैज्ञानिक आधार--------------------------------
आज विज्ञान का युग है और विज्ञान युग भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया है। हम अंतरिक्ष की बात ना भी करे परंतु पृथ्वी के बात तो हमें करनी ही होगी। विज्ञान ने हमें अंधविश्वास की दुनिया से निकल कर अनुभूत ज्ञान को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त किया है। आज किसी भी समाज के शिक्षा के उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी से भी प्रभावित होते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के कई मूल आधार है जिसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित किए जाते हैं।
